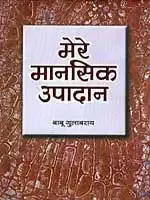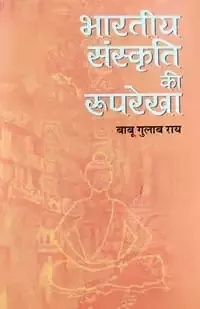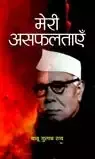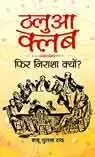|
लेख-निबंध >> मेरे मानसिक उपादान मेरे मानसिक उपादानबाबू गुलाबराय
|
298 पाठक हैं |
||||||
मेरे मानसिक उपादान..
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
निवेदन
बाबू गुलाबराय का हिन्दी साहित्य जगत् में निबंधकार और समीक्षक के रूप में
एक विशिष्ट स्थान है। बाबूजी ने साहित्यशास्त्र के सैद्धांतिक निबंधों के
अतिरिक्त विचारात्मक, व्यवहारिक और ललित-निबंध भी लिखे हैं। बाबूजी ने
साहित्यशास्त्र के सैद्धांतिक निबंधों के अतिरिक्त विचारात्मक, व्यावहारिक
और ललित-निबंध भी लिखे हैं। बाबूजी साहित्य और दर्शन के विद्वान थे,
अतः उनके निबंधों में दार्शनिक दृष्टि और निर्मल ज्ञान की अभिव्यक्ति मिलती है। बाबूजी ने जटिल-से-जटिल विषय को अपनी सरल, सर्वग्राह्य व सुबोध भाषा-शैली में बना दिया है। हिंदी में आचार्य रामचंद शुक्ल के पश्चात् बाबूजी ऐसे निबंधकार हैं जिनकी रचनाएँ आधुनिक युग में और अब भी प्रचार में हैं। उनका व्यक्तित्व उनके निबंधों में परिलक्षित होता है। बाबूजी के दो निबंध-संग्रह’ मेरे मानसिक उपादान’ जिसमें नैतिक और जीवन मीमांसा संबंधी, वैयक्तिक, राजनीतिक और यात्रा संबंधी निबंध है। इन सभी निबंधों में जीवन और जगत से प्राप्त उनकी अपनी अनुभूतियाँ हैं।
बाबूजी ने अपने निबंधों के विषय में लिखा है—‘‘सज्जन और सज्जनता में मेरे जीवन संबंधी आदर्श हैं। यद्यपि मैं स्वयं उन आदर्शों का पालन करने में असमर्थ रहा हूँ, तथापि यदि दूसरे सज्जन उसका पालन कर सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे जीवन आदर्श धर्म, अर्थ, काम के समन्वय से प्रभावित हैं। मेरे ये निबंध—विशेष कर यह निबंध, जो घरेलू लड़ाई-झगड़ों से संबंधित हैं—उन लोगों के लिए हैं, जिनके घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। वे अपने पारस्परिक प्रेम सद्भाव में वृद्धि कर उन्हें स्वर्णरंजित बना सकते हैं। कुछ निजी वैयक्तिक संबंध भी हैं।
यद्यपि मेरे सभी निबंधों में थोड़ा-बहुत वैयक्तिक पुट रहता है, तथापि इनमें विषय और शैली दोनों में ही व्यक्ति की प्रधानता है। मेरे राजनीतिक निबंध भी मेरे जीवन-दर्शन से प्रभावित हैं। राजनीति पर मैंने कम लिखा है; जो कुछ लिखा है, वह सद्भावना मात्र है। मैंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया,
इससे मुझे राजनीति पर कहने या लिखने का कोई अधिकार नहीं है। सद्भावनाओं की मुझमें कमी नहीं रही। देश के लिए कुछ बलिदान न कर सका, इसका मुझे खेद है।’’
इस संग्रह के कुछ निबंध में उन्होंने देश की दयनीय दशा का वास्तविक चित्र खींचा है। अंग्रेजी शासनकाल में देश परतंत्र था तथा अधिकांश देशवासियों के रहन—सहन का स्तर अत्यंत निम्न था। जिन लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा था, उनका नैतिक पतन हो चुका था। उन्हें विदेशी वस्तुएँ प्रिय थीं।
इन सब बातों को बाबूजी ने अपने उक्त निबंधों में दरशाया है। वैयक्तिक निबंधकार के रूप में बाबूजी सर्वाधिक सफल और अग्रणी रहे हैं। वैयक्तिक निबंधों में उनका जीवन, उनकी आत्मा, उनकी अपनी अनुभूतियाँ और विचार संकलित हैं। ऐसा ही एक लेख है इस संग्रह में ‘मेरे मानसिक उपादान’, जिसमें बाबूजी के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। आशा है, यह निबंध-संग्रह पाठकों को रुचिकर लगेगा और इसका प्रकाशन हिंदी-जगत में बाबू गुलाबरायजी की स्मृति को पुनः ताजा करेगा।
अतः उनके निबंधों में दार्शनिक दृष्टि और निर्मल ज्ञान की अभिव्यक्ति मिलती है। बाबूजी ने जटिल-से-जटिल विषय को अपनी सरल, सर्वग्राह्य व सुबोध भाषा-शैली में बना दिया है। हिंदी में आचार्य रामचंद शुक्ल के पश्चात् बाबूजी ऐसे निबंधकार हैं जिनकी रचनाएँ आधुनिक युग में और अब भी प्रचार में हैं। उनका व्यक्तित्व उनके निबंधों में परिलक्षित होता है। बाबूजी के दो निबंध-संग्रह’ मेरे मानसिक उपादान’ जिसमें नैतिक और जीवन मीमांसा संबंधी, वैयक्तिक, राजनीतिक और यात्रा संबंधी निबंध है। इन सभी निबंधों में जीवन और जगत से प्राप्त उनकी अपनी अनुभूतियाँ हैं।
बाबूजी ने अपने निबंधों के विषय में लिखा है—‘‘सज्जन और सज्जनता में मेरे जीवन संबंधी आदर्श हैं। यद्यपि मैं स्वयं उन आदर्शों का पालन करने में असमर्थ रहा हूँ, तथापि यदि दूसरे सज्जन उसका पालन कर सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे जीवन आदर्श धर्म, अर्थ, काम के समन्वय से प्रभावित हैं। मेरे ये निबंध—विशेष कर यह निबंध, जो घरेलू लड़ाई-झगड़ों से संबंधित हैं—उन लोगों के लिए हैं, जिनके घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। वे अपने पारस्परिक प्रेम सद्भाव में वृद्धि कर उन्हें स्वर्णरंजित बना सकते हैं। कुछ निजी वैयक्तिक संबंध भी हैं।
यद्यपि मेरे सभी निबंधों में थोड़ा-बहुत वैयक्तिक पुट रहता है, तथापि इनमें विषय और शैली दोनों में ही व्यक्ति की प्रधानता है। मेरे राजनीतिक निबंध भी मेरे जीवन-दर्शन से प्रभावित हैं। राजनीति पर मैंने कम लिखा है; जो कुछ लिखा है, वह सद्भावना मात्र है। मैंने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया,
इससे मुझे राजनीति पर कहने या लिखने का कोई अधिकार नहीं है। सद्भावनाओं की मुझमें कमी नहीं रही। देश के लिए कुछ बलिदान न कर सका, इसका मुझे खेद है।’’
इस संग्रह के कुछ निबंध में उन्होंने देश की दयनीय दशा का वास्तविक चित्र खींचा है। अंग्रेजी शासनकाल में देश परतंत्र था तथा अधिकांश देशवासियों के रहन—सहन का स्तर अत्यंत निम्न था। जिन लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा था, उनका नैतिक पतन हो चुका था। उन्हें विदेशी वस्तुएँ प्रिय थीं।
इन सब बातों को बाबूजी ने अपने उक्त निबंधों में दरशाया है। वैयक्तिक निबंधकार के रूप में बाबूजी सर्वाधिक सफल और अग्रणी रहे हैं। वैयक्तिक निबंधों में उनका जीवन, उनकी आत्मा, उनकी अपनी अनुभूतियाँ और विचार संकलित हैं। ऐसा ही एक लेख है इस संग्रह में ‘मेरे मानसिक उपादान’, जिसमें बाबूजी के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। आशा है, यह निबंध-संग्रह पाठकों को रुचिकर लगेगा और इसका प्रकाशन हिंदी-जगत में बाबू गुलाबरायजी की स्मृति को पुनः ताजा करेगा।
विनोद शंकर गुप्त
सज्जन और सज्जनता
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो
वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः।
तीर्णाः स्वयंभीमभवार्णवं
जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः।।*
वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः।
तीर्णाः स्वयंभीमभवार्णवं
जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः।।*
शिष्टाचार की भाषा में तो सभी लोग सज्जन हैं। ‘सीयराम मय सब जग
जानी’ के एकात्मवादपरक सिद्धांत के अनुयायी संतों और भक्तों की
दृष्टि इससे भिन्न नहीं है, किंतु व्यावहारित दृष्टि से सज्जनों और खलों
में भेद है। संसार में जो यत्किंचित् साम्य की स्थिति हैं, वह सज्जनों की
सज्जनता के कारण ही है। संसार की इस साम्यमयी स्थित को बनाए रखने और उसमें
अभिवृद्धि करने के लिए महापुरुषों और महाकवियों ने लोकहिताय सज्जनों के
लक्षण बताए हैं, यहाँ तक कि काव्य-शास्त्र के आचार्यों ने सज्जनों के
लक्षणों को महाकाव्य के वर्ण्य विषयों में प्रमुख स्थान दिया है।
‘श्रीमद्भागवद्गीता’ में स्थितप्रज्ञ, दैवी सम्पदा और भक्तों के लक्षण बताते हुए सज्जनता के आवश्यक उपकरणों पर प्रकाश डाला गया है। भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अमर कृति ‘रामचरितमानस’ में कई स्थानों पर संतों और सज्जनों के लक्षण बताए हैं। उनकी ‘विनयपत्रिका’ के ‘कबहुँक हौं यह रहनि रहौंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें संत स्वभाव गहौंगो’ से आरंभ होनेवाले प्रसिद्ध पद में जो जीवनादर्श उपस्थित किया गया है, उसमें सज्जनता की ही व्याख्या की गई है।
‘वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाणे रे’ वाले महात्मा गांधी के प्रिय भजन में वैष्णव भक्त के गुणों के मिस सज्जनों के ही गुण बताए गए हैं। प्रभु ईसा मसीह ने अपने ‘सरमन ऑन द माउंट’ में सज्जनों को ईश्वर के कृपापात्र बताते
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
इस भयंकर संसार-सागर से स्वयं तरे हुए शांत और महान् सज्जन पुरुष वसंत के समान लोक-हित करते हुए बिना कारण दूसरे लोगों को तारते हुए निवास करते हैं।
हुए उनका गुणगान किया है। कार्डीनैल न्यूमैन में अपनी ‘आइडिया ऑव एन यूनिवर्सिटी’ नामक अमूल्य पुस्तक में सज्जन (जेंटिलमैन) की परिभाषा दी है। सज्जनों के लक्षण अगणित हैं। स्वयं भगवान रामचंद्र ने अपने श्रीमुख से कहा है—‘संतन्ह के लच्छन सुन भ्राता। अगनित श्रुति पुरान विख्याता।।’ सज्जनता की परंपरा बहुत लंबी है। सारा साहित्य उसी ओर लक्ष्य करता है।
‘श्रीमद्भागवद्गीता’ में स्थितप्रज्ञ, दैवी सम्पदा और भक्तों के लक्षण बताते हुए सज्जनता के आवश्यक उपकरणों पर प्रकाश डाला गया है। भक्त-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी अमर कृति ‘रामचरितमानस’ में कई स्थानों पर संतों और सज्जनों के लक्षण बताए हैं। उनकी ‘विनयपत्रिका’ के ‘कबहुँक हौं यह रहनि रहौंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें संत स्वभाव गहौंगो’ से आरंभ होनेवाले प्रसिद्ध पद में जो जीवनादर्श उपस्थित किया गया है, उसमें सज्जनता की ही व्याख्या की गई है।
‘वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाणे रे’ वाले महात्मा गांधी के प्रिय भजन में वैष्णव भक्त के गुणों के मिस सज्जनों के ही गुण बताए गए हैं। प्रभु ईसा मसीह ने अपने ‘सरमन ऑन द माउंट’ में सज्जनों को ईश्वर के कृपापात्र बताते
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
इस भयंकर संसार-सागर से स्वयं तरे हुए शांत और महान् सज्जन पुरुष वसंत के समान लोक-हित करते हुए बिना कारण दूसरे लोगों को तारते हुए निवास करते हैं।
हुए उनका गुणगान किया है। कार्डीनैल न्यूमैन में अपनी ‘आइडिया ऑव एन यूनिवर्सिटी’ नामक अमूल्य पुस्तक में सज्जन (जेंटिलमैन) की परिभाषा दी है। सज्जनों के लक्षण अगणित हैं। स्वयं भगवान रामचंद्र ने अपने श्रीमुख से कहा है—‘संतन्ह के लच्छन सुन भ्राता। अगनित श्रुति पुरान विख्याता।।’ सज्जनता की परंपरा बहुत लंबी है। सारा साहित्य उसी ओर लक्ष्य करता है।
परहित-निरत
सज्जनो का सबसे बड़ा लक्षण है कि वे परहित के सदा अभिलाषी रहते हैं।
गोस्वामी तुलसीदासजी के शब्दों में उनकी अभिलाषा यही रहती है
‘पर
हित-निरत-निरंतर मन-क्रम-बचन नेम निबहौंगो’ वे सर्व वेद-पुराणों
के
सार-स्वरूप व्यासजी के ‘वचनद्वय’ पर आधारित
‘परहित सरसि
धर्म नहिं भाई, परपीड़ा सम नहिं अधमाई’ वाले सिद्धांत को कभी
नहीं
भूलते। हित और अनहित के विचार में असावधानी नहीं करते हैं।
हित की बात को सामने रखते हुए किसी आतंकवाद से काम न लेंगे। वे समझाने-बुझाने द्वारा व्यक्ति को सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करने में अधिक विश्वास करते हैं।
सज्जनों का सारा जीवन ही परोपकार के लिए होता है—‘परोपकाराय सतां विभूतयः।’ गोस्वामी तुलसीदासजी ने परोपकार को श्रुति का सार कहा है और उसमें नर तनु की सार्थकता मानी है-
हित की बात को सामने रखते हुए किसी आतंकवाद से काम न लेंगे। वे समझाने-बुझाने द्वारा व्यक्ति को सत्कार्यों की ओर प्रवृत्त करने में अधिक विश्वास करते हैं।
सज्जनों का सारा जीवन ही परोपकार के लिए होता है—‘परोपकाराय सतां विभूतयः।’ गोस्वामी तुलसीदासजी ने परोपकार को श्रुति का सार कहा है और उसमें नर तनु की सार्थकता मानी है-
काज कहा नर तनु धरि सार्यौं।
पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखेहु न विचार्यौ।।
पर उपकार सार श्रुति को जो, सो धोखेहु न विचार्यौ।।
वे ‘आत्मानः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्’ की नीति
का
निर्वाह करते हैं। वे पराए दुःख में दुःखी और पराए सुख में सुखी होते
हैं-
विषय अलंपट सील गुनाकर।
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर।।
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर।।
उपकृत का मान
सज्जन उपकार करते हुए भी अपने को ही उपकृत समझते हैं। योगीराज भगवान्
श्रीकृष्ण ने ‘आर्त’ और
‘अर्थार्थी’ भक्तों को भी
उदार कहा है—‘उदाराः सर्व एवैते’। सज्जन
याचक को
यथासंभव ‘नाहीं’ नहीं करते; ‘उनसे पहले वे
मुए जिन मुख
निकसत नाहिं’। वे याचक को दान से ही नहीं वरन् मान से भी
संतुष्ट
करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्रजी के विषय में कहा गया है कि
उन्होंने याचकों को ‘दान मान संतोषे’। सज्जन भगवान्
रामचंद्र
के इसी गुण को अपनाने में सुख का अनुभव करते हैं। रामभक्त सबको मान देता
हुआ आप अमानी रहती है—‘सबहिं मानप्रद आप
अमानी।
निरभिमानता
‘विगत मान सम सीतल मन’ सज्जनों को अभिमान छू तक नहीं
जाता।
‘मन अभिमान न आणे रे’। वे अपने को निमित्त मात्र
समझते हैं।
वे अपने में कर्ता बुद्धि को आने नहीं देते। उनकी आँखें सदा नीची रहती
हैं—‘‘अधोऽधः पश्यतः कस्य महिमा
नोपजायते’। अहसान
जताना तो दूर, वे उन संकेतों एवं लाक्षणिक और व्यंजनात्मक वाक्यों को
जिह्वाग्र पर नहीं आने देते, जिनसे कि दूसरे को हीनता का अनुभव नहीं करने
देते। स्वंय ही दूसरों की आवश्यकता—पूर्ति के साधन जुटा देते
हैं।
अस को उदार जग माहीं।
बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहिं।।
बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहिं।।
सज्जन राम के इसी गुण का अनुसरण करता है, फिर भी निरभिमान रहता है। वह
अपने किए हुए का श्रेय दूसरों को देता है। श्रीकृष्णजी ने गोवर्धन पर्वत
को उठाने में ग्वाल-बालों का सहयोग लिया और उनको श्रेय दिया। दावानल को
बुझाकर भी कह दिया कि घास,-फूस की आग थी, अपने आप बुझ गई।’
‘द्वारिकाधीश’ के पद से भी दीन सुदामा के पैर
पखारे—‘पानी परात को हाथ छुओ नहिं, नैनन के जल सों पग
धोए।
परनिंदा-विवर्जन
सज्जन पराई निंदा से बचता है। वह अपवादों के सुनने में अपना समय नष्ट नहीं
करता। वह लोगों की कमजोरियों की सहानुभूति की दृष्टि से देखता है। पराई
निंदा सुनना तो जहाँ-तहाँ रहा, गोस्वामीजी के शब्दों में कपास की भाँति
‘जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा’ की नीति को अपनाता है,
वह महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए तीन बंदरों की भाँति दूसरों की बुराई के लिए आँखों, कानों और मुँह पर हाथ रखे रहता है। वह दूसरों की बुराई न देखेगा, न सुनेगा और न कहेगा। वह पराए अवगुणों को नहीं वरन् गुणों को देखता है, पर गुन नहिं दोष कहौगो’। पराई बुराई का सुनना और कहना गोस्वामीजी ने खलों का लक्षण बतलाया है। खलों की वंदना करते हुए उन्होंने कहा है-
वह महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए तीन बंदरों की भाँति दूसरों की बुराई के लिए आँखों, कानों और मुँह पर हाथ रखे रहता है। वह दूसरों की बुराई न देखेगा, न सुनेगा और न कहेगा। वह पराए अवगुणों को नहीं वरन् गुणों को देखता है, पर गुन नहिं दोष कहौगो’। पराई बुराई का सुनना और कहना गोस्वामीजी ने खलों का लक्षण बतलाया है। खलों की वंदना करते हुए उन्होंने कहा है-
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book